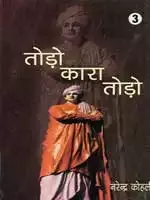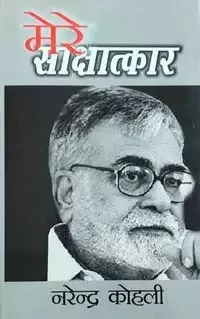|
बहुभागीय पुस्तकें >> तोड़ो, कारा तोड़ो - 3 तोड़ो, कारा तोड़ो - 3नरेन्द्र कोहली
|
179 पाठक हैं |
||||||
तीसरा खंड ‘परिव्राजक’
इस पुस्तक का सेट खरीदें।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पिछले दस वर्षों में लोकप्रियता के नए कीर्तीमान स्थापित करने वाली रचना
तोड़ो, कारा तोड़ो नरेन्द्र कोहली की नवीनतम उपन्यास-श्रृंखला है। यह
शीर्षक रवीन्द्र ठाकुर के गीत की एक पंक्ति का अनुवाद है। किंतु उपन्यास
का संबंध स्वामी विवेकानन्द की जीवनकथा से है। स्वामी विवेकानन्द का जीवन
बंधनों तथा सीमाओं के अत्क्रमण के लिए सार्थक संधर्ष थाः बंधन चाहे
प्रकृति केस हों, समाज के हों, राजनीतिक के हों, धर्म के हों, अध्यात्म के
हों। नरेन्द्र कोहली के ही शब्दों में, ‘‘स्वामी
विवेकानन्द के व्यक्तित्व का आकर्षक...आकर्षक नहीं, जादू....जादू जो सिर
चढ़कर बोलता है। कोई संवेदनशील व्यक्ति उनके निकट जाकर सम्मोहित हुए बिना
नहीं रह सकता।...और युवा मन तो उत्साह से पागल ही हो जाता है। कौन-सा गुण
था, जो स्वामी जी में नहीं था। मानव के चरम विकास की साक्षात् मूर्ति थे
वे। भारत की आत्मा...और वे एकाकार हो गये थे। उन्हें किसी एक युग, प्रदेश
संप्रदाय अथवा संगठन के साथ बाँध देना अज्ञान भी है और अन्याय
भी।’’ ऐसे स्वामी विवेकानन्द के साथ तादात्म्य किया
है नरेन्द्र कोहली ने। उनका यह उपन्यास ऐसा ही तादात्म्य करा देता है,
पाठक का उस विभूति से।
इस बृहत् उपन्यास का प्रथम खंड ‘निर्माण’ स्वामी जी के व्यक्तित्व के निर्माण के विभिन्न आयामों तथा चरणों की कथा कहता है। इसका क्षेत्र उनके जन्म से लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस तथा जगन्माता भवतारिणी के सम्मुख निर्द्वंद्व आत्मसमर्पण तक की घटनाओं पर आधृत है।
दूसरा खंड ‘साधना’ अपने गुरु के चरणों में बैठकर की गयी साधना और गुरु के शरीर-त्याग के पश्चात् उनके आदेशानुसार, अपने गुरुभाइयों को एक मठ में संगठित करने की कथा है।
तीसरे खंड ‘परिव्राजक’ में उनके एक अज्ञात संन्यासी के रूप में, कलकत्ता से द्वारका तक के भ्रमण की कथा है।
‘निर्देश’, ‘तोड़ो, कारा तोड़ो’ का चौथा खंड है।
द्वारका में सागर-तट पर बैठकर स्वामी विवेकानन्द ने भारत-माता की दुर्दशा पर अश्रु बहाए थे। वे एक नया संकल्प लेकर उठे और वडोदरा के महाराज गायकवाड़ से मिलने के लिए आए। वे अनुभव कर रहे थे कि उन्हें अलौकिक निर्देश मिले रहे हैं कि वे एक विशेष लक्ष्य से इस संसार में आए हैं।
विभिन्न देशी राज्यों और रजवाड़ों में होते हुए वे कन्याकुमारी पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी तीन दिनों की समाधि में जगदंबा और भारत माता के दर्शन एक साथ किए। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उन्हें अपने मोक्ष के लिए तपस्या करने के स्थान पर भारतमाता और उनकी संतानों की सेवा करनी है।
रामेश्वरम् के दर्शन कर वे मद्रास पहुँच गए। मद्रास में नव युवकों के एक संगठित दल ने उन्हें शिकागो में होने वाली धर्मसंसद में भेजने का निश्चय किया और उसके लिए तैयारी आरंभ कर दी। किंतु स्वामी जी इस बात पर अड़े हुए थे कि वे अपनी इच्छा से नहीं, माँ के आदेश से शिकागों जाएँगे। अतः माँ अपनी इच्छा प्रकट करे। अंततः माँ ने अपनी इच्छा का ‘निर्देश’ किया। स्वामी जी ने शिकागो तक की यात्रा की। स्वामीजी और उनको भेजने वाले शिष्य-दोनों ही अनुभवहीन थे। अतः स्वामी जी अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फँस गए, किंतु जगदंबा ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे संसद में भाग ले सके और विदेशियों तथा विधर्मियों द्वारा भारतमाता की छवि पर पोते गए अपमान के कीचड़ को धोकर उसके सौंदर्य को संसार के सम्मुख प्रस्तुत कर सके। इस सफलता ने स्वामी जी को अनेक मित्र और अनेक शक्तिशाली शत्रु दिए। उन्हें परेशान किया गया, कलंकित किया गया और अंततः उनकी हत्या का प्रयत्न किया गया। स्वामी जी ने जगदंबा के निर्देश, अपने गुरु के संरक्षण और अपने संकल्प से उन सब कठिनाइयों का सामना किया और संसार को भारत का संदेश देने में जुट गए।
स्वामी विवेकानन्द का जीवन निकट अतीत की घटना है। उनके जीवन में प्रायः घटनाएँ सप्रमाण इतिहासांकित हैं। यहाँ उपन्यास कार के लिए अपनी कल्पना अथवा अपने चितंन को आरोपति करने की सुविधा नहीं है। उपन्यासकार को वही कहना होगा, जो स्वामी जी ने कहा था। अपने नायक के व्यक्तित्व और चिंतन से तादाम्त्य ही उसके लिए एक मात्र मार्ग है।
नरेन्द्र कोहली ने अपने नायक को उनकी परंपरा तथा उनके परिवेश से पृथक कर नहीं देखा। स्वामी विवेकानन्द ऐसे नायक हैं भी नहीं, जिन्हें अपने परिवेश से अलग-थलग किया जा सके। वे तो जैसे महासागर के किसी असाधारण ज्वार के उद्दामतम चरम अंश थे। तोड़ो, कारा तोड़ों उस ज्वार को पूर्ण रुप से जीवंत करने का औपन्यासिक प्रयत्न है, जो स्वामी जी को उनके पूर्वापर के मध्य रखकर ही देखना चाहता है। अतः इस उपन्यास के लिए न श्री रामकृष्ण पराए हैं, न स्वामीजी के सहयोगी, गुरुभाई और न ही उनकी शिष्य-परंपरा की प्रतीक भगिनी निवेदिता।
इस बृहत् उपन्यास का प्रथम खंड ‘निर्माण’ स्वामी जी के व्यक्तित्व के निर्माण के विभिन्न आयामों तथा चरणों की कथा कहता है। इसका क्षेत्र उनके जन्म से लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस तथा जगन्माता भवतारिणी के सम्मुख निर्द्वंद्व आत्मसमर्पण तक की घटनाओं पर आधृत है।
दूसरा खंड ‘साधना’ अपने गुरु के चरणों में बैठकर की गयी साधना और गुरु के शरीर-त्याग के पश्चात् उनके आदेशानुसार, अपने गुरुभाइयों को एक मठ में संगठित करने की कथा है।
तीसरे खंड ‘परिव्राजक’ में उनके एक अज्ञात संन्यासी के रूप में, कलकत्ता से द्वारका तक के भ्रमण की कथा है।
‘निर्देश’, ‘तोड़ो, कारा तोड़ो’ का चौथा खंड है।
द्वारका में सागर-तट पर बैठकर स्वामी विवेकानन्द ने भारत-माता की दुर्दशा पर अश्रु बहाए थे। वे एक नया संकल्प लेकर उठे और वडोदरा के महाराज गायकवाड़ से मिलने के लिए आए। वे अनुभव कर रहे थे कि उन्हें अलौकिक निर्देश मिले रहे हैं कि वे एक विशेष लक्ष्य से इस संसार में आए हैं।
विभिन्न देशी राज्यों और रजवाड़ों में होते हुए वे कन्याकुमारी पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी तीन दिनों की समाधि में जगदंबा और भारत माता के दर्शन एक साथ किए। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उन्हें अपने मोक्ष के लिए तपस्या करने के स्थान पर भारतमाता और उनकी संतानों की सेवा करनी है।
रामेश्वरम् के दर्शन कर वे मद्रास पहुँच गए। मद्रास में नव युवकों के एक संगठित दल ने उन्हें शिकागो में होने वाली धर्मसंसद में भेजने का निश्चय किया और उसके लिए तैयारी आरंभ कर दी। किंतु स्वामी जी इस बात पर अड़े हुए थे कि वे अपनी इच्छा से नहीं, माँ के आदेश से शिकागों जाएँगे। अतः माँ अपनी इच्छा प्रकट करे। अंततः माँ ने अपनी इच्छा का ‘निर्देश’ किया। स्वामी जी ने शिकागो तक की यात्रा की। स्वामीजी और उनको भेजने वाले शिष्य-दोनों ही अनुभवहीन थे। अतः स्वामी जी अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फँस गए, किंतु जगदंबा ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे संसद में भाग ले सके और विदेशियों तथा विधर्मियों द्वारा भारतमाता की छवि पर पोते गए अपमान के कीचड़ को धोकर उसके सौंदर्य को संसार के सम्मुख प्रस्तुत कर सके। इस सफलता ने स्वामी जी को अनेक मित्र और अनेक शक्तिशाली शत्रु दिए। उन्हें परेशान किया गया, कलंकित किया गया और अंततः उनकी हत्या का प्रयत्न किया गया। स्वामी जी ने जगदंबा के निर्देश, अपने गुरु के संरक्षण और अपने संकल्प से उन सब कठिनाइयों का सामना किया और संसार को भारत का संदेश देने में जुट गए।
स्वामी विवेकानन्द का जीवन निकट अतीत की घटना है। उनके जीवन में प्रायः घटनाएँ सप्रमाण इतिहासांकित हैं। यहाँ उपन्यास कार के लिए अपनी कल्पना अथवा अपने चितंन को आरोपति करने की सुविधा नहीं है। उपन्यासकार को वही कहना होगा, जो स्वामी जी ने कहा था। अपने नायक के व्यक्तित्व और चिंतन से तादाम्त्य ही उसके लिए एक मात्र मार्ग है।
नरेन्द्र कोहली ने अपने नायक को उनकी परंपरा तथा उनके परिवेश से पृथक कर नहीं देखा। स्वामी विवेकानन्द ऐसे नायक हैं भी नहीं, जिन्हें अपने परिवेश से अलग-थलग किया जा सके। वे तो जैसे महासागर के किसी असाधारण ज्वार के उद्दामतम चरम अंश थे। तोड़ो, कारा तोड़ों उस ज्वार को पूर्ण रुप से जीवंत करने का औपन्यासिक प्रयत्न है, जो स्वामी जी को उनके पूर्वापर के मध्य रखकर ही देखना चाहता है। अतः इस उपन्यास के लिए न श्री रामकृष्ण पराए हैं, न स्वामीजी के सहयोगी, गुरुभाई और न ही उनकी शिष्य-परंपरा की प्रतीक भगिनी निवेदिता।
परिव्राजक
‘‘मास्टर मोशाय आए हैं माँ !’’
दस वर्षीय भूपेन्द्र ने आकर भुवनेश्वरी को सूचना दी।
‘‘तू यहाँ दादा के पास बैठ। मैं उनसे बात कर अभी आती हूँ।’’ भुवनेश्वरी कुछ असमंजस में थी, ‘‘जाने क्या कहने आये हैं। नरेन्द्र तो यहाँ है भी नहीं कि उससे दो बातें करने आए हों।’’
भुवनेश्वरी कमरे से बाहर आ गईं। द्वार से निकलते हुए उन्होंने देखा कि महेन्द्रनाथ गुप्त बरामदे में बिछे तख्तपोश पर बैठे कोई पुस्तक देख रहे थे। संभवतः वे भूपेन्द्र और महेश की ही पुस्तकें होंगी, जो वे उनके आने से पहले पढ़ रहे थे और अब उन्हें वहीं छोड़ गए थे।
‘‘नमस्कार !’’
महेन्द्र गुप्त ने भुवनेश्वरी को आते देखा तो बहुत सम्मानपूर्वक उठ खड़े हुए।
‘‘नमस्कार ।’’ वे बोलीं, ‘‘कैसे हैं आप ?’’
‘‘ठाकुर की कृपा है।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त बोले, ‘‘आप लोग सब सकुशल तो हैं न ?’’
‘‘मास्टर मोशाय ! मैं तो नहीं कहूँगी कि भगवान् की हम पर कृपा नहीं है। कृतघ्न नहीं हूं मैं।’’ भुवनेश्वरी बोलीं, ‘‘उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। नरेन्द्र जैसा पुत्र है। किंतु यह आपसे भी छिपा नहीं है कि हमारी स्थिति कैसी है। जिस स्त्री के पति का देहान्त हो गया हो; पिता के पश्चात जिसे परिवार का बोझ उठाना था, वह बड़ा पुत्र संन्यासी हो गया हो; और सारे सगे-संबंधी वैरी हो गए हों, वह स्त्री अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ कैसी हो सकती है। हाँ इतनी तो भगवान् की कृपा रही कि अपने पति के देहांत से पहले मेरी पुत्रियाँ अपनी-अपनी ससुराल चली गईं।...छोड़िए।’’ भुवनेश्वरी ने विषय बदल दिया, ‘‘कहिए, नरेन्द्र कैसा है ? आप उससे मिलते ही होंगे उसने कोई संदेश भेजा है क्या ?’’
‘‘नहीं। इधर कुछ दिनों से उससे मेरी भेंट नहीं हुई है।’’ वे बोले, ‘‘वैसे आशा करनी चाहिए कि स्वस्थ और प्रसन्न ही होगा।’’
भुवनेश्वरी को लगा कि मास्टर मोशाय के स्वर में न तो सामान्य सहजता है और न ही आत्मबल। इसका अर्थ है जो कुछ वे कह रहे हैं, उसमें तो कुछ झूठ नहीं है; किन्तु जो सत्य भुवनेश्वरी को अप्रिय हो सकता था, उसे वे कह नहीं रहे। नहीं कह रहे हैं तो न सही...भुवनेश्वरी ने मन में सोचा ....उन्हें भी किसी रहस्य का उद्घाटन तो करवाना नहीं है। जो कुछ महेन्द्रनाथ गुप्त कहने आए हैं, उसे कहे बिना तो नहीं ही लौटेंगे।...
‘‘कोई विशेष बात कहने आये हैं या हमारा हालचाल जानने....?’’ वे बोलीं, ‘‘चाय पिएँगे आप ?’’
महेन्द्रनाथ गुप्त को कुछ बल मिला, ‘‘नहीं, चाय नहीं पियूँगा। किंतु मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ।’’
भुवनेश्वरी कुछ चकित हुई, ‘‘कैसी याचना ?’’ उन्होंने स्वयं को सँभाला, ‘‘कहिए ! आपकी याचना से मुझे बल मिलेगा कि मैं अब भी किसी का कोई काम करने में समर्थ हूं।’’ उनके चेहरे पर उभरी मुस्कान में निहित कटुता का तत्त्व कोई भी स्पष्ट पहचान सकता था।
‘‘मैं श्रीमाँ के दर्शनों के लिए गया था।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त बोले, ‘‘उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहीं से नरेन्द्र का चित्र उन्हें उपलब्ध करा दूँ।....
‘‘क्यों, चित्र का क्या करेंगी ?’’ भुवनेश्वरी ने कहा, ‘‘जब स्वयं नरेन्द्र उन्हीं के पास है तो वे चित्र का क्या करेंगी ?’’
‘‘वे अपने उस प्रिय पुत्र का चित्र अपने पास रखना चाहती हैं।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त जैसे साँस लेकर बोले, ‘‘सब समय तो पुत्र निकट नहीं होता न !’’
‘‘नरेन्द्र उनके पास है,।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त को अंततः कहना ही पड़ा; किंतु उनका स्वर जैसे कुछ सहम गया था।
‘‘हाँ ! हाँ ! उनके पास नहीं है, मठ में है।’’ भुवनेश्वरी ने महेन्द्रनाथ के स्वर तथा मुद्रा-परिवर्तन पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, ‘‘पर उनको प्रणाम करने जाता होगा। अपनी गुरुपत्नी के पालन-पोषण करने का प्रबन्ध करने जाता होगा। वे स्वयं भी मठ में जा सकती हैं। मेरे समान मठ में जाने पर उनके लिए कोई प्रतिबन्ध तो नहीं है। मैं तो स्त्री मात्र हूँ, वे तो गुरुपत्नी हैं। मैं कोई नहीं हूँ, वे श्रीमाँ हैं। स्वयं न जाना चाहें तो वे मठ में संदेश भेज सकती हैं।....
‘‘बात यह है दीदी !’’ महेन्द्रनाथ गुप्त बोले, ‘‘नरेन्द्र परिव्राजक के रूप में देश-भ्रमण के लिए चला गया है।’’
‘‘तो आ जाएगा पहले भी कई बार जा चुका है।’’
‘‘नहीं। इस बार वह अज्ञात काल के लिए गया है। जाने कब लौटे...यदि कहीं उससे किसी कारण से वापस न लौटने का संकल्प कर लिया तो नहीं लौट सकता...
भुवनेश्वरी का मुख जैसे आश्चर्य से खुल गया..यह मास्टर मोशाय क्या कह रहे हैं, उनको पता भी है !
‘‘यह सब आप किस आधार पर कह रहे हैं ?’’ भुवनेश्वरी का स्वर कुछ उत्तेजित था।
‘‘नरेन्द्र अपने प्रस्थान से पहले आशीर्वाद लेने श्रीमाँ के पास गया था। उसी ने कुछ इस प्रकार के संकेत दिए थे, जिनसे श्रीमाँ आशंकित हैं।’’
‘‘वे उसे समझा नहीं सकती थीं कि ऐसी मूर्खता वह न करे !’’ भुवनेश्वरी बोलीं, ‘‘मेरी बात तो वह सुनता ही नहीं है; किंतु अपनी गुरुपत्नी के आदेश को टालने का साहस वह नहीं कर सकता।’’
‘‘आप ठीक कह रही हैं।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त ने कहा, ‘‘श्रीमाँ ने उसे समझाया था और उसने वचन लिया था कि वह ऐसा संकल्प नहीं करेगा। उसने भी हँसकर शीघ्र लौटाने का वचन दिया है।....’’
‘‘तो वे उसका चित्र क्यों चाहती हैं ?’’
‘‘जब तक वह लौटकर नहीं आता, तब तक के लिए भी कोई आधार होना चाहिए।’’ भुवनेश्वरी कुछ सोचती रहीं। फिर धीरे से बोलीं, ‘‘वह जाने से पहले मुझसे अनुमति या आशीर्वाद लेने क्यों नहीं आया ? मेरे आशीर्वाद की अब उसे आवश्यकता नहीं है ?
मुझे सूचना क्यों नहीं भिजवाई ?’’
महेन्द्रनथ गुप्त सिर झुकाए बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, ‘‘श्रीमाँ ने उससे पूछा था कि क्या वह आपसे आशीर्वाद लेने नहीं जाएगा ? तो उसने कहा...’’
‘‘क्या कहा ?’’
‘‘कहा कि श्रीमाँ के अतिरिक्त उसकी और कोई माँ नहीं है।’’
‘‘मैं उसकी कोई नहीं हूँ ? जिसने उसे काशीनाथ वीरेश्वर महादेव से आँचल फैलाकर माँगा, जिसने उसे जन्म दिया, पालन-पोषण किया, मैं अब उसकी कोई नहीं हूँ ?’’ उनके स्वर में आक्रोश था, ‘‘तुम्हारी उस श्रीमाँ ने नरेन्द्र के लिए क्या किया है कि वे ही अब उसकी सब कुछ हो गईं ?’’ महेन्द्रनाथ गुप्त सिर झुकाए हुए ही कहा, ‘‘आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप जानती ही हैं कि संन्यासी का अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। वह अपने सारे रिश्ते-नाते तोड़कर केवल ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले साधकों से अपना संबंध मानता है। साधना की यात्रा में गुरु और गुरुपत्नी का महत्त्व तो आप जानती हैं ?’’
‘‘गुरुपत्नी वैसे तो गुरु की उत्तराधिकारिणी होती ही है; किंतु हमारे लिए तो ठाकुर के बाद अब श्रीमाँ उनकी प्रतिमूर्ति ही हैं।’’
‘‘मेरे श्वसुर भी संन्यासी हो गए थे। उन्होंने भी अपने परिवार, यहाँ तक की अपनी निर्दोष किंतु दुखी पत्नी तक से संबंध तोड़ लिया था।’’ भुवनेश्वरी ने महेन्द्रनाथ गुप्त की ओर देखा, ‘‘किंतु मास्टर मोशाय ! मेरी समझ में एक बात नहीं आती।’’
‘‘क्या दीदी ?’’
‘‘जब किसी से संबंध रखना ही है तो उन्हीं से क्यों न रखा जाए जिनसे भगवान ने हमारा संबंध बनाया है ? एक माँ आपको चाहिए तो उसी माँ को माँ क्यों नहीं माना जाए, जिसने हमें जन्म दिया है ?’’ भुवनेश्वरी बोलीं, ‘‘नैसर्गिक संबंधों को तोड़कर कृमिक संबंध की क्या सार्थकता है ? अपनी माँ को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए और किसी और स्त्री को माँ कहकर उसकी सेवा की जाए....’’
‘‘देखिए, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो इन संन्यासियों के साथ रहकर उनको देख-देखकर कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त बोले, ‘‘किंतु इतना कह सकता हूँ कि देह-संबंधों में मोह होता है, जबकि साधक के संबंध में केवल श्रद्धा या स्नेह होता है।’’
‘‘देह-संबंध...’’
‘‘अपने नरेन्द्र को ही नहीं, महेन्द्र और भूपेन्द्र को भी जन्म दिया है। वे आपकी देह से उत्पन्न हुए हैं। आपका उन सबसे मोहजनित स्नेह है। सबको होता है। हमको अपना स्नेह दिखाई देता है, उसमें छिपा मोह नहीं। ठाकुर अथवा श्रीमाँ को नरेन्द्र ही प्रिय है, महेन्द्र या भूपेन्द्र से उनका कोई संबंध नहीं है। यह ईश्वरीय या साधनात्मक संबंध है। देह का संबंध तो सांसारिक संबंध है। उसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। नरेन्द्र एक भजन गाया करता था तुलसीदास का-‘जाको प्रिय न राम वैदेही ! तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जदपि परम स्नेही।’ आप मुझसे अधिक जानती ही हैं दीदी ! संसार जिसे ग्रहण करने को कहता है, अध्यात्म उसे त्यागने को कहता है। और मैं समझता हूँ कि नरेन्द्र को और उसके कारण आप लोगों को जो कष्ट सहने पड़े हैं, वे भगवान् की ओर से नरेन्द्र की परीक्षा थी। अपने माँ-बाप को दुखी और संपन्न देखकर, उनको त्यागने में उतना कष्ट नहीं होता; किंतु दुःख की ऐसी घड़ी में उन्हें छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़ना साधारण साहस का काम नहीं है।’’
‘‘जानती हूँ।’’ भुवनेश्ररी ने कुछ सोचते हुए बहुत धीरे से कहा।
‘‘जिस युग में एक सर्वथा अपढ़-अशिक्षित भी अपनी आजीविका कमा लेता है, उस युग में नरेन्द्र जैसे विद्वान् को आजीविका नहीं मिली। जिस देश में लूले लँगड़े का भी विवाह हो जाता है, वहाँ नरेन्द्र जैसे सुदर्शन, बलवान और मेधावी युवक का विवाह नहीं हुआ।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त ने कहा,
‘‘ये सब ईश्वरीय संदेश नहीं हैं कि नरेन्द्र को संन्यासी ही बनना था।’’
‘‘संन्यासी बनने के लिए ही जन्मा था वह।’’
‘‘तो उसकी परीक्षा भी होनी ही थी और वह परीक्षा उसने दी। सबसे मोह तोड़कर चला गया।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त ने कुछ रुककर कहा, ‘‘दीदी ! आप यह न समझें कि वह केवल घरवालों के प्रति ही निर्मम हुआ है। वह तो अपने गुरुभाइयों से भी अपना संबंध तोड़ रहा है। वह कहता है कि वह एक परिवार से मोह तोड़कर दूसरे परिवार के प्रति नया मोह नहीं पालना चाहता।’’
‘‘ठीक कहता है।’’
‘‘हाँ, कहता तो ठीक ही है।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त ने कहा, ‘‘मठ में भी सब लोग आशंकित हैं। श्रीमाँ ने गंगाधर को नरेन्द्र के साथ भेजा है कि कहीं नरेन्द्र संपर्क के सारे सूत्र छिन्न-भिन्न न कर डाले।’’
‘‘नरेन्द्र सबको छोड़ सकता है तो क्या एक गंगाधर को नहीं छोड़ सकता ?’’ भुवनेश्वरी बोलीं, ‘‘राम सारे अयोध्यावासियों को श्रृंगवेरपुर में सोते छोड़कर चले गए थे। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को सोते छोड़ गए थे। नरेन्द्र गंगाधर को छोड़ना चाहेगा तो किसी भी युक्ति से उसे छोड़ जाएगा।’’ भुवनेश्वरी ने रुककर महेन्द्र गुप्त की ओर देखा, ‘‘मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए मास्टर मोशाय !’’
महेन्द्रनाथ गुप्त की प्रश्नवाचक दृष्टि उनकी ओर उठी।
‘‘नरेन्द्र ने संन्यास लिया है, मैंने नहीं। वह मुझे अपनी माँ माने न माने, मैं उसको अपना पुत्र ही मानती हूँ। सबसे बडा पुत्र है मेरा; और अपने गुणों के कारण वह मुझे सबसे अधिक प्रिय भी है। शायद उसे अपना पुत्र मानती हैं, यह प्रसन्नता का विषय है। वे उसकी माँ बनना चाहती हैं, बनें। कोई मेरे पुत्र को प्रेम करता है, तो वह मुझे बुरा क्यों लगेगा ? किंतु यह कभी न भूलें कि मैं नरेन्द्र की जननी हूँ। मैंने उसे जन्म दिया है। कोई योगी हो, संन्यासी हो, किंतु भगवान् के बनाए इस संबंध से इंकार नहीं कर सकता। शंकराचार्य को भी अंत में अपनी माँ के पास लौटना पड़ा था।...यदि उन्हें उसका कोई समाचार मिले, कोई संदेश मिले तो मुझे उसकी सूचना अवश्य दें।’’
‘‘अवश्य दीदी ! मैं उनसे कह दूँगा। मठ के संन्यासियों को भी कह दूँगा और स्वयं भी ध्यान रखूँगा।’’ वे रुके, ‘‘वैसे मैं जानता हूँ कि नरेन्द्र न आपकी उपेक्षा करेगा, न आपकी ओर से असावधान रहेगा।’’
‘‘कैसे कह सकते हैं आप ?’’
‘‘मुझे बताया गया है कि जब तक ठाकुर ने उसे उसके परिवार के लिए मोटे अन्न और वस्त्र की ओर से निश्चिंत नहीं कर दिया, उसने संन्यास ग्रहण नहीं किया।’’
‘‘सुना है मैंने भी।’’
दोनों कुछ देर मौन रहे, फिर महेन्द्र गुप्त ही बोले, ‘‘दीदी ! वह चित्र ?’’
‘‘देती हूँ।’’ भुवनेश्वरी उठकर भीतर चली गईं, जाने वह इस समय कहाँ होगा और क्या कह रहा होगा !
‘‘तू यहाँ दादा के पास बैठ। मैं उनसे बात कर अभी आती हूँ।’’ भुवनेश्वरी कुछ असमंजस में थी, ‘‘जाने क्या कहने आये हैं। नरेन्द्र तो यहाँ है भी नहीं कि उससे दो बातें करने आए हों।’’
भुवनेश्वरी कमरे से बाहर आ गईं। द्वार से निकलते हुए उन्होंने देखा कि महेन्द्रनाथ गुप्त बरामदे में बिछे तख्तपोश पर बैठे कोई पुस्तक देख रहे थे। संभवतः वे भूपेन्द्र और महेश की ही पुस्तकें होंगी, जो वे उनके आने से पहले पढ़ रहे थे और अब उन्हें वहीं छोड़ गए थे।
‘‘नमस्कार !’’
महेन्द्र गुप्त ने भुवनेश्वरी को आते देखा तो बहुत सम्मानपूर्वक उठ खड़े हुए।
‘‘नमस्कार ।’’ वे बोलीं, ‘‘कैसे हैं आप ?’’
‘‘ठाकुर की कृपा है।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त बोले, ‘‘आप लोग सब सकुशल तो हैं न ?’’
‘‘मास्टर मोशाय ! मैं तो नहीं कहूँगी कि भगवान् की हम पर कृपा नहीं है। कृतघ्न नहीं हूं मैं।’’ भुवनेश्वरी बोलीं, ‘‘उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। नरेन्द्र जैसा पुत्र है। किंतु यह आपसे भी छिपा नहीं है कि हमारी स्थिति कैसी है। जिस स्त्री के पति का देहान्त हो गया हो; पिता के पश्चात जिसे परिवार का बोझ उठाना था, वह बड़ा पुत्र संन्यासी हो गया हो; और सारे सगे-संबंधी वैरी हो गए हों, वह स्त्री अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ कैसी हो सकती है। हाँ इतनी तो भगवान् की कृपा रही कि अपने पति के देहांत से पहले मेरी पुत्रियाँ अपनी-अपनी ससुराल चली गईं।...छोड़िए।’’ भुवनेश्वरी ने विषय बदल दिया, ‘‘कहिए, नरेन्द्र कैसा है ? आप उससे मिलते ही होंगे उसने कोई संदेश भेजा है क्या ?’’
‘‘नहीं। इधर कुछ दिनों से उससे मेरी भेंट नहीं हुई है।’’ वे बोले, ‘‘वैसे आशा करनी चाहिए कि स्वस्थ और प्रसन्न ही होगा।’’
भुवनेश्वरी को लगा कि मास्टर मोशाय के स्वर में न तो सामान्य सहजता है और न ही आत्मबल। इसका अर्थ है जो कुछ वे कह रहे हैं, उसमें तो कुछ झूठ नहीं है; किन्तु जो सत्य भुवनेश्वरी को अप्रिय हो सकता था, उसे वे कह नहीं रहे। नहीं कह रहे हैं तो न सही...भुवनेश्वरी ने मन में सोचा ....उन्हें भी किसी रहस्य का उद्घाटन तो करवाना नहीं है। जो कुछ महेन्द्रनाथ गुप्त कहने आए हैं, उसे कहे बिना तो नहीं ही लौटेंगे।...
‘‘कोई विशेष बात कहने आये हैं या हमारा हालचाल जानने....?’’ वे बोलीं, ‘‘चाय पिएँगे आप ?’’
महेन्द्रनाथ गुप्त को कुछ बल मिला, ‘‘नहीं, चाय नहीं पियूँगा। किंतु मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ।’’
भुवनेश्वरी कुछ चकित हुई, ‘‘कैसी याचना ?’’ उन्होंने स्वयं को सँभाला, ‘‘कहिए ! आपकी याचना से मुझे बल मिलेगा कि मैं अब भी किसी का कोई काम करने में समर्थ हूं।’’ उनके चेहरे पर उभरी मुस्कान में निहित कटुता का तत्त्व कोई भी स्पष्ट पहचान सकता था।
‘‘मैं श्रीमाँ के दर्शनों के लिए गया था।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त बोले, ‘‘उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहीं से नरेन्द्र का चित्र उन्हें उपलब्ध करा दूँ।....
‘‘क्यों, चित्र का क्या करेंगी ?’’ भुवनेश्वरी ने कहा, ‘‘जब स्वयं नरेन्द्र उन्हीं के पास है तो वे चित्र का क्या करेंगी ?’’
‘‘वे अपने उस प्रिय पुत्र का चित्र अपने पास रखना चाहती हैं।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त जैसे साँस लेकर बोले, ‘‘सब समय तो पुत्र निकट नहीं होता न !’’
‘‘नरेन्द्र उनके पास है,।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त को अंततः कहना ही पड़ा; किंतु उनका स्वर जैसे कुछ सहम गया था।
‘‘हाँ ! हाँ ! उनके पास नहीं है, मठ में है।’’ भुवनेश्वरी ने महेन्द्रनाथ के स्वर तथा मुद्रा-परिवर्तन पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, ‘‘पर उनको प्रणाम करने जाता होगा। अपनी गुरुपत्नी के पालन-पोषण करने का प्रबन्ध करने जाता होगा। वे स्वयं भी मठ में जा सकती हैं। मेरे समान मठ में जाने पर उनके लिए कोई प्रतिबन्ध तो नहीं है। मैं तो स्त्री मात्र हूँ, वे तो गुरुपत्नी हैं। मैं कोई नहीं हूँ, वे श्रीमाँ हैं। स्वयं न जाना चाहें तो वे मठ में संदेश भेज सकती हैं।....
‘‘बात यह है दीदी !’’ महेन्द्रनाथ गुप्त बोले, ‘‘नरेन्द्र परिव्राजक के रूप में देश-भ्रमण के लिए चला गया है।’’
‘‘तो आ जाएगा पहले भी कई बार जा चुका है।’’
‘‘नहीं। इस बार वह अज्ञात काल के लिए गया है। जाने कब लौटे...यदि कहीं उससे किसी कारण से वापस न लौटने का संकल्प कर लिया तो नहीं लौट सकता...
भुवनेश्वरी का मुख जैसे आश्चर्य से खुल गया..यह मास्टर मोशाय क्या कह रहे हैं, उनको पता भी है !
‘‘यह सब आप किस आधार पर कह रहे हैं ?’’ भुवनेश्वरी का स्वर कुछ उत्तेजित था।
‘‘नरेन्द्र अपने प्रस्थान से पहले आशीर्वाद लेने श्रीमाँ के पास गया था। उसी ने कुछ इस प्रकार के संकेत दिए थे, जिनसे श्रीमाँ आशंकित हैं।’’
‘‘वे उसे समझा नहीं सकती थीं कि ऐसी मूर्खता वह न करे !’’ भुवनेश्वरी बोलीं, ‘‘मेरी बात तो वह सुनता ही नहीं है; किंतु अपनी गुरुपत्नी के आदेश को टालने का साहस वह नहीं कर सकता।’’
‘‘आप ठीक कह रही हैं।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त ने कहा, ‘‘श्रीमाँ ने उसे समझाया था और उसने वचन लिया था कि वह ऐसा संकल्प नहीं करेगा। उसने भी हँसकर शीघ्र लौटाने का वचन दिया है।....’’
‘‘तो वे उसका चित्र क्यों चाहती हैं ?’’
‘‘जब तक वह लौटकर नहीं आता, तब तक के लिए भी कोई आधार होना चाहिए।’’ भुवनेश्वरी कुछ सोचती रहीं। फिर धीरे से बोलीं, ‘‘वह जाने से पहले मुझसे अनुमति या आशीर्वाद लेने क्यों नहीं आया ? मेरे आशीर्वाद की अब उसे आवश्यकता नहीं है ?
मुझे सूचना क्यों नहीं भिजवाई ?’’
महेन्द्रनथ गुप्त सिर झुकाए बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, ‘‘श्रीमाँ ने उससे पूछा था कि क्या वह आपसे आशीर्वाद लेने नहीं जाएगा ? तो उसने कहा...’’
‘‘क्या कहा ?’’
‘‘कहा कि श्रीमाँ के अतिरिक्त उसकी और कोई माँ नहीं है।’’
‘‘मैं उसकी कोई नहीं हूँ ? जिसने उसे काशीनाथ वीरेश्वर महादेव से आँचल फैलाकर माँगा, जिसने उसे जन्म दिया, पालन-पोषण किया, मैं अब उसकी कोई नहीं हूँ ?’’ उनके स्वर में आक्रोश था, ‘‘तुम्हारी उस श्रीमाँ ने नरेन्द्र के लिए क्या किया है कि वे ही अब उसकी सब कुछ हो गईं ?’’ महेन्द्रनाथ गुप्त सिर झुकाए हुए ही कहा, ‘‘आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप जानती ही हैं कि संन्यासी का अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। वह अपने सारे रिश्ते-नाते तोड़कर केवल ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले साधकों से अपना संबंध मानता है। साधना की यात्रा में गुरु और गुरुपत्नी का महत्त्व तो आप जानती हैं ?’’
‘‘गुरुपत्नी वैसे तो गुरु की उत्तराधिकारिणी होती ही है; किंतु हमारे लिए तो ठाकुर के बाद अब श्रीमाँ उनकी प्रतिमूर्ति ही हैं।’’
‘‘मेरे श्वसुर भी संन्यासी हो गए थे। उन्होंने भी अपने परिवार, यहाँ तक की अपनी निर्दोष किंतु दुखी पत्नी तक से संबंध तोड़ लिया था।’’ भुवनेश्वरी ने महेन्द्रनाथ गुप्त की ओर देखा, ‘‘किंतु मास्टर मोशाय ! मेरी समझ में एक बात नहीं आती।’’
‘‘क्या दीदी ?’’
‘‘जब किसी से संबंध रखना ही है तो उन्हीं से क्यों न रखा जाए जिनसे भगवान ने हमारा संबंध बनाया है ? एक माँ आपको चाहिए तो उसी माँ को माँ क्यों नहीं माना जाए, जिसने हमें जन्म दिया है ?’’ भुवनेश्वरी बोलीं, ‘‘नैसर्गिक संबंधों को तोड़कर कृमिक संबंध की क्या सार्थकता है ? अपनी माँ को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए और किसी और स्त्री को माँ कहकर उसकी सेवा की जाए....’’
‘‘देखिए, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो इन संन्यासियों के साथ रहकर उनको देख-देखकर कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त बोले, ‘‘किंतु इतना कह सकता हूँ कि देह-संबंधों में मोह होता है, जबकि साधक के संबंध में केवल श्रद्धा या स्नेह होता है।’’
‘‘देह-संबंध...’’
‘‘अपने नरेन्द्र को ही नहीं, महेन्द्र और भूपेन्द्र को भी जन्म दिया है। वे आपकी देह से उत्पन्न हुए हैं। आपका उन सबसे मोहजनित स्नेह है। सबको होता है। हमको अपना स्नेह दिखाई देता है, उसमें छिपा मोह नहीं। ठाकुर अथवा श्रीमाँ को नरेन्द्र ही प्रिय है, महेन्द्र या भूपेन्द्र से उनका कोई संबंध नहीं है। यह ईश्वरीय या साधनात्मक संबंध है। देह का संबंध तो सांसारिक संबंध है। उसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। नरेन्द्र एक भजन गाया करता था तुलसीदास का-‘जाको प्रिय न राम वैदेही ! तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जदपि परम स्नेही।’ आप मुझसे अधिक जानती ही हैं दीदी ! संसार जिसे ग्रहण करने को कहता है, अध्यात्म उसे त्यागने को कहता है। और मैं समझता हूँ कि नरेन्द्र को और उसके कारण आप लोगों को जो कष्ट सहने पड़े हैं, वे भगवान् की ओर से नरेन्द्र की परीक्षा थी। अपने माँ-बाप को दुखी और संपन्न देखकर, उनको त्यागने में उतना कष्ट नहीं होता; किंतु दुःख की ऐसी घड़ी में उन्हें छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़ना साधारण साहस का काम नहीं है।’’
‘‘जानती हूँ।’’ भुवनेश्ररी ने कुछ सोचते हुए बहुत धीरे से कहा।
‘‘जिस युग में एक सर्वथा अपढ़-अशिक्षित भी अपनी आजीविका कमा लेता है, उस युग में नरेन्द्र जैसे विद्वान् को आजीविका नहीं मिली। जिस देश में लूले लँगड़े का भी विवाह हो जाता है, वहाँ नरेन्द्र जैसे सुदर्शन, बलवान और मेधावी युवक का विवाह नहीं हुआ।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त ने कहा,
‘‘ये सब ईश्वरीय संदेश नहीं हैं कि नरेन्द्र को संन्यासी ही बनना था।’’
‘‘संन्यासी बनने के लिए ही जन्मा था वह।’’
‘‘तो उसकी परीक्षा भी होनी ही थी और वह परीक्षा उसने दी। सबसे मोह तोड़कर चला गया।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त ने कुछ रुककर कहा, ‘‘दीदी ! आप यह न समझें कि वह केवल घरवालों के प्रति ही निर्मम हुआ है। वह तो अपने गुरुभाइयों से भी अपना संबंध तोड़ रहा है। वह कहता है कि वह एक परिवार से मोह तोड़कर दूसरे परिवार के प्रति नया मोह नहीं पालना चाहता।’’
‘‘ठीक कहता है।’’
‘‘हाँ, कहता तो ठीक ही है।’’ महेन्द्रनाथ गुप्त ने कहा, ‘‘मठ में भी सब लोग आशंकित हैं। श्रीमाँ ने गंगाधर को नरेन्द्र के साथ भेजा है कि कहीं नरेन्द्र संपर्क के सारे सूत्र छिन्न-भिन्न न कर डाले।’’
‘‘नरेन्द्र सबको छोड़ सकता है तो क्या एक गंगाधर को नहीं छोड़ सकता ?’’ भुवनेश्वरी बोलीं, ‘‘राम सारे अयोध्यावासियों को श्रृंगवेरपुर में सोते छोड़कर चले गए थे। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को सोते छोड़ गए थे। नरेन्द्र गंगाधर को छोड़ना चाहेगा तो किसी भी युक्ति से उसे छोड़ जाएगा।’’ भुवनेश्वरी ने रुककर महेन्द्र गुप्त की ओर देखा, ‘‘मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए मास्टर मोशाय !’’
महेन्द्रनाथ गुप्त की प्रश्नवाचक दृष्टि उनकी ओर उठी।
‘‘नरेन्द्र ने संन्यास लिया है, मैंने नहीं। वह मुझे अपनी माँ माने न माने, मैं उसको अपना पुत्र ही मानती हूँ। सबसे बडा पुत्र है मेरा; और अपने गुणों के कारण वह मुझे सबसे अधिक प्रिय भी है। शायद उसे अपना पुत्र मानती हैं, यह प्रसन्नता का विषय है। वे उसकी माँ बनना चाहती हैं, बनें। कोई मेरे पुत्र को प्रेम करता है, तो वह मुझे बुरा क्यों लगेगा ? किंतु यह कभी न भूलें कि मैं नरेन्द्र की जननी हूँ। मैंने उसे जन्म दिया है। कोई योगी हो, संन्यासी हो, किंतु भगवान् के बनाए इस संबंध से इंकार नहीं कर सकता। शंकराचार्य को भी अंत में अपनी माँ के पास लौटना पड़ा था।...यदि उन्हें उसका कोई समाचार मिले, कोई संदेश मिले तो मुझे उसकी सूचना अवश्य दें।’’
‘‘अवश्य दीदी ! मैं उनसे कह दूँगा। मठ के संन्यासियों को भी कह दूँगा और स्वयं भी ध्यान रखूँगा।’’ वे रुके, ‘‘वैसे मैं जानता हूँ कि नरेन्द्र न आपकी उपेक्षा करेगा, न आपकी ओर से असावधान रहेगा।’’
‘‘कैसे कह सकते हैं आप ?’’
‘‘मुझे बताया गया है कि जब तक ठाकुर ने उसे उसके परिवार के लिए मोटे अन्न और वस्त्र की ओर से निश्चिंत नहीं कर दिया, उसने संन्यास ग्रहण नहीं किया।’’
‘‘सुना है मैंने भी।’’
दोनों कुछ देर मौन रहे, फिर महेन्द्र गुप्त ही बोले, ‘‘दीदी ! वह चित्र ?’’
‘‘देती हूँ।’’ भुवनेश्वरी उठकर भीतर चली गईं, जाने वह इस समय कहाँ होगा और क्या कह रहा होगा !
2
1890 ई० के अगस्त का पहला सप्ताह था। प्रातः अच्छी वर्षा हुई थी और अब
बादलों का छँट जाना अच्छा लगा रहा था।
मन्मथनाथ चौधरी दोपहर के भोजन के पश्चात् अपने बँगले के खुले बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठे थे। यहाँ से गंगा की धारा भली प्रकार दिखाई दे रही थी। बंगाली होते हुए भी मन्मथ बाबू की सदा से ही मान्यता रही थी कि भागलपुर में गंगा का जल और दृष्य-दोनों ही कलकत्ता की गंगा से अधिक सुंदर हैं।..किंतु इस समय उनका ध्यान गंगा की ओर न होकर, अपने सामने बैठे दो संन्यासियों पर टिका था और वे बुरी तरह खीजे हुए थे।...
ब्राह्म धर्म क्यों स्वीकार किया था उन्होंने ? इसलिए कि इन पाखंडी हिंदू साधुओं का सत्कार करते रहें। इन्हीं का सत्कार करना था तो हिंदू धर्म त्यागने का क्या अर्थ ? और फिर साधु भी कैसे ? भगवा धारण कर भिक्षा माँगने वाले। अनपढ़ लट्ठ भिखारियों को वे साधुओं का सम्मान कैसे दे सकते थे ? कैसे मान लें कि वे संत हैं ?...
...प्रातः राजा शिवचंद्र के पुत्र कुमार नित्यानन्द सिंह इन साधुओं को मन्मथ बाबू को यह कहकर सौंप गए थे कि उनसे कुमार की भेंट प्रातः गंगातट हुई थी और कुमार उन दोनों की असाधारणता से बहुत प्रभावित हुए थे।...
अब कुमार का मन्मथ बाबू क्या करते ? सुबह की सुबह आकर इन दो भिखमंगों को उनकी छाती पर बैठा गए। श्रावण का महीना है। वर्षा होती ही रहती है। बाहर खुले में कहाँ रहेंगे ये लोग ? कुमार को जाने किस व्यक्ति में क्या गुण दिखाई दे जाए ? कह गए-‘ये दोनों बहुत गुणी साधु हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप इनकी देखभाल करें।...
मन्मथ बाबू के मन में तत्काल विरोध उभरा था। पूछना चाहते थे कि गुणी साधु हैं तो कुमार उन्हें अपने ही महल में क्यों ठहरा नहीं लेते ? किंतु अपनी शालीनता में वे पूछ नहीं पाए।’’ पर शायद कुमार ने उनका आशय भाँप लिय़ा था..या संभव है कि उनके अपने मन में ही आया हो, इसलिए बता दिया...‘मैं इन्हें अपने ही घर ले जाता; किंतु जब जाना कि बंगाली हैं, तो सोचा, कदाचित् आपके यहाँ अधिक सुखी रहेंगे। आपकी भाषा-बोली एक है। खान-पान भी एक है..। मछली-वछली...वैसे कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहें।...’
कुमार ने जब इतना कुछ कह दिया था तो मन्मथ बाबू के पास कहने को कुछ विशेष नहीं था।...फिर एक वाक्य मन में आया भी..भागलपुर में वे ही तो अकेले बंगाली नहीं थे। ढेर बंगाली बसे हुए थे यहाँ।...और ‘बंगाली’ के नाम पर उसके मन में बेहद कटुता जागी...वे स्वयं ही आज तक इस द्वंद्व से निकल नहीं पाए थेः ब्राह्म को जानने के कारण वे मांसाहार छोड़ दें या बंगाली होने के नाते मछली खाते रहें।....और ये साधु भी बनेंगे और मछली का स्वाद भी लेंगे।...
पर कुछ कह नहीं पाए। बाध्यता में इन अनचाहे अतिथियों को स्वीकार कर लिया।...उद्दंड हो आए विद्रोही मन को समझा दिया..इतना बड़ा घर है, कहीं पड़े रहेंगे। जहाँ इतने लोग खाते हैं, इन दोनों के भात का भी प्रबंध हो ही जाएगा।...पर वे इन्हें अधिक दिन टिकने नहीं देंगे...यह निश्चय वे पहले ही कर चुके थे ।...
कुमार के जाने के पश्चात् अपने ढंग से उन्होंने संन्यासियों के सम्मुख अपना विरोध जता दिया था, ‘‘शायद आप
लोग हिंदू हैं। सनातनी हिंदू।’’
‘‘सुविधा के लिए यही मान लीजिए।’’ उनमें से एक ने कहा था।
‘‘किंतु मैं ब्राह्म हूँ’’ मन्मथ बाबू ने कुछ कठोर होने का प्रयत्न किया था, ‘‘आप जानते हैं कि ब्राह्म लोग हिंदू नहीं होते। मुझे हिंदू शास्त्रों पर तनिक भी श्रद्धा नहीं है।’’
संन्यासियों ने मुस्कराकर वह सूचना स्वीकार कर ली थी। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। मन्थन बाबू को लगा, उनकी नीति सफल नहीं हुई। उन्हें कुछ अधिक प्रहारक होना चाहिए था।
‘‘मेरे घर में भोजन से आपका धर्म भ्रष्ट तो नहीं होगा ?’’ अपनी वाणी की वक्रता से वे स्वयं ही सहम गए थे।
‘‘हमारी मान्यता ऐसी नहीं हैं।’’ पहले संन्यासी ने पुनः कहा, ‘‘वैसे यह आचार-विचार गृहस्थों का है। संन्यासी सामाजिक बंधनों से मुक्त होता है।’’
‘‘हाँ।’’ मन्मथ बाबू सोच रहे थे, ‘फोकट में भोजन पाना हो तो इस प्रकार के आदर्श बघारने चाहिए।’ बोले, ‘‘किंतु धार्मिक बंधनों से तो मुक्त नहीं होता संन्यासी।’’
‘‘नहीं।’’
‘‘तो विधर्मी के घर भोजन से आपका धर्म रोकता नहीं आपको ?’’
‘‘धर्म जाति-पाँति तथा विभिन्न संप्रदायों का भेद नहीं मानता।’’ वहीं संन्यासी पुनः बोला,
‘‘यह व्यवस्था समाज की है। सच पूछिए तो समाज की भी नहीं हैं, व्यवसायों की है। विभिन्न व्यवसाय करने वालों ने अपनी-अपनी बिरादरी बना ली और समाज ने उनके सामर्थ्य और साधन-संपन्नता इत्यादि के अनुसार उनमें एक प्रकार की व्यवस्था स्थापित कर दी। धर्म का इनसे कुछ लेना-देना नहीं है।’’
मन्मथ बाबू संन्यासी की बात की कोई तर्कसंगत काट नहीं खोज पाए; किंतु संन्यासी के तर्क को स्वीकार करने का उनका तनिक भी मन नहीं हुआ।...मान लिया कि यह संन्यासी की चतुराई मात्र थी। यदि वह इस व्यवस्था को धर्मसंगत मान लेता, तो उसे अपने भोजन की व्यवस्था कहीं और करनी पड़ती...
‘‘कहाँ की यात्रा कर रहें है आप ?’’ मन्मथ बाबू ने पूछा।
‘‘हिमालय क्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘तपस्या के विचार से।’’
‘‘क्यों, कलकत्ता में तपस्या नहीं हो सकती ?’’
संन्यासी की आँखों में जो भाव आया, उसकी ध्वनि स्पष्ट थी वह उसका अभिप्राय समझ रहा है। बोला, ‘‘अब तक जो कुछ किया है, कलकत्ता में ही किया है; किंतु कलकत्ता में घर-परिवार, मित्र-बंधु, गुरुभाई बहुत निकट हैं। वहाँ साधक का मोह नहीं छूटता। संन्यासी का मोहमुक्त होना बहुत आवश्यक है कि साधक एकांतवास करे, या कम से कम से कम अपने प्रियजनों से तो दूर ही रहे।’’
मन्मथ बाबू को जैसे अपने मतलब का सूत्र मिल गया, ‘‘किस परिवार के हैं आप ? आपके माता-पिता कौन हैं ? कहाँ रहते हैं ?’’
संन्यासी बहुत सधे हुए ढंग से मुस्कराया, ‘‘संन्यासी से उसके पूर्व आश्रम और अतीत के विषय में कुछ नहीं पूछना चाहिए।’’
संन्यासी ने अपने एक ही वाक्य से उन्हें निरस्त कर दिया था, किंतु मन्मथ बाबू उससे प्रभावित नहीं, आहत हुए थे। मान लिया कि यह भिखमंगा बहुत चतुर है। शब्द-चातुरी में पारंगत है। अपने व्यवसाय के सारे मंत्र जानता है। इससे और वार्तालाप का कोई लाभ नहीं था।...
मन्मथ बाबू ने उन्हें भोजन करवा दिया था, किंतु संन्यासियों का इस प्रकार उनके सामने बैठे रहना उन्हें तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था।..उनका मन जल रहा था...आश्रय दिया है तो इसका यह अर्थ तो नहीं है कि वे लोग उनके परिवार के सम्मानित अतिथि हो गए ! उनके घर में जब चाहें, जहाँ चाहें, आ जा सकते हैं। उनके अतिथियों के साथ बैठ सकते हैं। उनके साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं। उनके एकांत में घुसपैठ कर सकते हैं...भगवा धारण कर लेने पर भिखमंगा, भिखमंगा नहीं रहता क्या ?...मन्मथ बाबू को लग रहा था कि वे उनके सामने कुर्सियों पर नहीं, उनके वक्ष पर ही जमें बैठे हैं।...कुमार नित्यानन्द सिंह की यह जबर्दस्ती वे जीवन-भर नहीं भुला पाएँगे।...
मन्मथ बाबू ने एक उचटती-सी दृष्टि उन पर डाली और अनमने-से बैठ गए। उन्हें टालने का एक ही मार्ग था कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। वे समझ रहे थे कि आगंतुकों के प्रति उनका व्यवहार बहुत शिष्ट नहीं था; किंतु वे क्या करते ? जो लोग उन्हें प्रिय नहीं लगते ? उनसे बात, करने के लिए उनके मन में कोई भाव ही नहीं उगता। और ये लोग तो बलात् उनके घर में घुस आए थे और अब उनके सामने आ बैठे थे।.... इतने ही साधु हैं तो जाएँ और अपने कमरे में ध्यान करें।...
मन्मथ बाबू ने पास रखी एक पुस्तक उठा ली...वे पढ़ते रहेंगे तो ये लोग अपनी उपेक्षा मानकर स्वयं ही उठ जाएँगे। रूठकर उनके घर से ही चले जाएँ तो और भी अच्छा है।...
‘‘आप यह कौन-सी पुस्तक पढ़ रहे हैं ?’’ सहसा पहले साधु ने सीधे मन्मथ बाबू से ही पूछ लिया। मन्मथ बाबू के मन में एक मिश्रित-सी प्रतिक्रया हुई....किंतु यही अवसर था कि वे उसे उसका स्थान दिखा सकते थे...
‘‘बौद्ध धर्म पर लिखी गई एक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद है।’’ मन्मथ बाबू के स्वर में स्पष्ट व्यंग्य था, ‘‘कुछ पढ़े-लिखे भी हैं ? अंग्रेजी आती है ?’’
‘‘थोड़ी-थोड़ी।’’ साधु मुस्कराकर बाँग्ला में ही बोला, ‘‘अंग्रेजी जानने से ही कोई पढ़ा लिखा हो जाता है ?’’
‘‘क्यों ? पढ़-लिखकर ही तो अंग्रेजी आती है।’’ मन्मथ बाबू ने कुछ आवेश में कहा ।
‘‘नहीं ऐसे बहुत सारे अंग्रेज और अमेरिकी है जो तनिक भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, किंतु उनको अंग्रेजी आती है।’’ साधु ने कहा।
मन्मथ बाबू ने ध्यान से साधु की ओर देखाः वह वैसा मूर्ख भिखारी नहीं था, जैसा मन्मथ बाबू समझे बैठे थे। फिर भी उनके पढ़े-लिखे होने की संभावना से मन्मथ बाबू को किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हुई। उलटे उनकी खीज की आग को हवा दे गई।...यह कैसे संभव है ?...संन्यासी होकर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ता; और अंग्रेजी पढ़कर कोई संन्यासी नहीं होता।...
‘‘ठीक है, पर भारत में ऐसा नहीं होता।’’ मन्मथ बाबू ने स्वयं को सँभाला, ‘‘मैं मान लेता हूँ कि आप पढ़े-लिखे हैं।...तो महात्मा बुद्ध के विषय में भी कुछ जानते होंगे ? नाम तो सुना ही होगा ?’’ उन्होंने प्रश्न अंग्रेजी में ही किया था। अभी इस पाखंडी की पोल खुल जाती है।
‘‘कौन हिंदू उनके विषय में नहीं जानता।’’ साधु ने अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की।
‘‘आपका उनके विषय में क्या विचार है ?’’ मन्मथ बाबू साधु को घेर लेना चाहते थे।
‘‘सर्वभूतों के प्रति और विशेष कर अज्ञानी और दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति में ही तथागत का महान् गौरव सन्निहित होता है।’’ संन्यासी ने परिष्कृत अंग्रेजी में कहा, ‘‘बुद्ध के धर्मोंपदेश के समय संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गई थी। वह उस समय केवल पंडितों के ग्रंथों की ही भाषा थी। बुद्धदेव के कुछ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत में करना चाहा था, पर बुद्धदेव उनसे सदा यही कहते, ‘‘मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ, अतः मुझे जनभाषा में ही बोलने दो।’ और उसी कारण से उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन भाषा में ही पाए जाते हैं।’’
मन्मथनाथ चौधरी दोपहर के भोजन के पश्चात् अपने बँगले के खुले बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठे थे। यहाँ से गंगा की धारा भली प्रकार दिखाई दे रही थी। बंगाली होते हुए भी मन्मथ बाबू की सदा से ही मान्यता रही थी कि भागलपुर में गंगा का जल और दृष्य-दोनों ही कलकत्ता की गंगा से अधिक सुंदर हैं।..किंतु इस समय उनका ध्यान गंगा की ओर न होकर, अपने सामने बैठे दो संन्यासियों पर टिका था और वे बुरी तरह खीजे हुए थे।...
ब्राह्म धर्म क्यों स्वीकार किया था उन्होंने ? इसलिए कि इन पाखंडी हिंदू साधुओं का सत्कार करते रहें। इन्हीं का सत्कार करना था तो हिंदू धर्म त्यागने का क्या अर्थ ? और फिर साधु भी कैसे ? भगवा धारण कर भिक्षा माँगने वाले। अनपढ़ लट्ठ भिखारियों को वे साधुओं का सम्मान कैसे दे सकते थे ? कैसे मान लें कि वे संत हैं ?...
...प्रातः राजा शिवचंद्र के पुत्र कुमार नित्यानन्द सिंह इन साधुओं को मन्मथ बाबू को यह कहकर सौंप गए थे कि उनसे कुमार की भेंट प्रातः गंगातट हुई थी और कुमार उन दोनों की असाधारणता से बहुत प्रभावित हुए थे।...
अब कुमार का मन्मथ बाबू क्या करते ? सुबह की सुबह आकर इन दो भिखमंगों को उनकी छाती पर बैठा गए। श्रावण का महीना है। वर्षा होती ही रहती है। बाहर खुले में कहाँ रहेंगे ये लोग ? कुमार को जाने किस व्यक्ति में क्या गुण दिखाई दे जाए ? कह गए-‘ये दोनों बहुत गुणी साधु हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप इनकी देखभाल करें।...
मन्मथ बाबू के मन में तत्काल विरोध उभरा था। पूछना चाहते थे कि गुणी साधु हैं तो कुमार उन्हें अपने ही महल में क्यों ठहरा नहीं लेते ? किंतु अपनी शालीनता में वे पूछ नहीं पाए।’’ पर शायद कुमार ने उनका आशय भाँप लिय़ा था..या संभव है कि उनके अपने मन में ही आया हो, इसलिए बता दिया...‘मैं इन्हें अपने ही घर ले जाता; किंतु जब जाना कि बंगाली हैं, तो सोचा, कदाचित् आपके यहाँ अधिक सुखी रहेंगे। आपकी भाषा-बोली एक है। खान-पान भी एक है..। मछली-वछली...वैसे कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहें।...’
कुमार ने जब इतना कुछ कह दिया था तो मन्मथ बाबू के पास कहने को कुछ विशेष नहीं था।...फिर एक वाक्य मन में आया भी..भागलपुर में वे ही तो अकेले बंगाली नहीं थे। ढेर बंगाली बसे हुए थे यहाँ।...और ‘बंगाली’ के नाम पर उसके मन में बेहद कटुता जागी...वे स्वयं ही आज तक इस द्वंद्व से निकल नहीं पाए थेः ब्राह्म को जानने के कारण वे मांसाहार छोड़ दें या बंगाली होने के नाते मछली खाते रहें।....और ये साधु भी बनेंगे और मछली का स्वाद भी लेंगे।...
पर कुछ कह नहीं पाए। बाध्यता में इन अनचाहे अतिथियों को स्वीकार कर लिया।...उद्दंड हो आए विद्रोही मन को समझा दिया..इतना बड़ा घर है, कहीं पड़े रहेंगे। जहाँ इतने लोग खाते हैं, इन दोनों के भात का भी प्रबंध हो ही जाएगा।...पर वे इन्हें अधिक दिन टिकने नहीं देंगे...यह निश्चय वे पहले ही कर चुके थे ।...
कुमार के जाने के पश्चात् अपने ढंग से उन्होंने संन्यासियों के सम्मुख अपना विरोध जता दिया था, ‘‘शायद आप
लोग हिंदू हैं। सनातनी हिंदू।’’
‘‘सुविधा के लिए यही मान लीजिए।’’ उनमें से एक ने कहा था।
‘‘किंतु मैं ब्राह्म हूँ’’ मन्मथ बाबू ने कुछ कठोर होने का प्रयत्न किया था, ‘‘आप जानते हैं कि ब्राह्म लोग हिंदू नहीं होते। मुझे हिंदू शास्त्रों पर तनिक भी श्रद्धा नहीं है।’’
संन्यासियों ने मुस्कराकर वह सूचना स्वीकार कर ली थी। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। मन्थन बाबू को लगा, उनकी नीति सफल नहीं हुई। उन्हें कुछ अधिक प्रहारक होना चाहिए था।
‘‘मेरे घर में भोजन से आपका धर्म भ्रष्ट तो नहीं होगा ?’’ अपनी वाणी की वक्रता से वे स्वयं ही सहम गए थे।
‘‘हमारी मान्यता ऐसी नहीं हैं।’’ पहले संन्यासी ने पुनः कहा, ‘‘वैसे यह आचार-विचार गृहस्थों का है। संन्यासी सामाजिक बंधनों से मुक्त होता है।’’
‘‘हाँ।’’ मन्मथ बाबू सोच रहे थे, ‘फोकट में भोजन पाना हो तो इस प्रकार के आदर्श बघारने चाहिए।’ बोले, ‘‘किंतु धार्मिक बंधनों से तो मुक्त नहीं होता संन्यासी।’’
‘‘नहीं।’’
‘‘तो विधर्मी के घर भोजन से आपका धर्म रोकता नहीं आपको ?’’
‘‘धर्म जाति-पाँति तथा विभिन्न संप्रदायों का भेद नहीं मानता।’’ वहीं संन्यासी पुनः बोला,
‘‘यह व्यवस्था समाज की है। सच पूछिए तो समाज की भी नहीं हैं, व्यवसायों की है। विभिन्न व्यवसाय करने वालों ने अपनी-अपनी बिरादरी बना ली और समाज ने उनके सामर्थ्य और साधन-संपन्नता इत्यादि के अनुसार उनमें एक प्रकार की व्यवस्था स्थापित कर दी। धर्म का इनसे कुछ लेना-देना नहीं है।’’
मन्मथ बाबू संन्यासी की बात की कोई तर्कसंगत काट नहीं खोज पाए; किंतु संन्यासी के तर्क को स्वीकार करने का उनका तनिक भी मन नहीं हुआ।...मान लिया कि यह संन्यासी की चतुराई मात्र थी। यदि वह इस व्यवस्था को धर्मसंगत मान लेता, तो उसे अपने भोजन की व्यवस्था कहीं और करनी पड़ती...
‘‘कहाँ की यात्रा कर रहें है आप ?’’ मन्मथ बाबू ने पूछा।
‘‘हिमालय क्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘तपस्या के विचार से।’’
‘‘क्यों, कलकत्ता में तपस्या नहीं हो सकती ?’’
संन्यासी की आँखों में जो भाव आया, उसकी ध्वनि स्पष्ट थी वह उसका अभिप्राय समझ रहा है। बोला, ‘‘अब तक जो कुछ किया है, कलकत्ता में ही किया है; किंतु कलकत्ता में घर-परिवार, मित्र-बंधु, गुरुभाई बहुत निकट हैं। वहाँ साधक का मोह नहीं छूटता। संन्यासी का मोहमुक्त होना बहुत आवश्यक है कि साधक एकांतवास करे, या कम से कम से कम अपने प्रियजनों से तो दूर ही रहे।’’
मन्मथ बाबू को जैसे अपने मतलब का सूत्र मिल गया, ‘‘किस परिवार के हैं आप ? आपके माता-पिता कौन हैं ? कहाँ रहते हैं ?’’
संन्यासी बहुत सधे हुए ढंग से मुस्कराया, ‘‘संन्यासी से उसके पूर्व आश्रम और अतीत के विषय में कुछ नहीं पूछना चाहिए।’’
संन्यासी ने अपने एक ही वाक्य से उन्हें निरस्त कर दिया था, किंतु मन्मथ बाबू उससे प्रभावित नहीं, आहत हुए थे। मान लिया कि यह भिखमंगा बहुत चतुर है। शब्द-चातुरी में पारंगत है। अपने व्यवसाय के सारे मंत्र जानता है। इससे और वार्तालाप का कोई लाभ नहीं था।...
मन्मथ बाबू ने उन्हें भोजन करवा दिया था, किंतु संन्यासियों का इस प्रकार उनके सामने बैठे रहना उन्हें तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था।..उनका मन जल रहा था...आश्रय दिया है तो इसका यह अर्थ तो नहीं है कि वे लोग उनके परिवार के सम्मानित अतिथि हो गए ! उनके घर में जब चाहें, जहाँ चाहें, आ जा सकते हैं। उनके अतिथियों के साथ बैठ सकते हैं। उनके साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं। उनके एकांत में घुसपैठ कर सकते हैं...भगवा धारण कर लेने पर भिखमंगा, भिखमंगा नहीं रहता क्या ?...मन्मथ बाबू को लग रहा था कि वे उनके सामने कुर्सियों पर नहीं, उनके वक्ष पर ही जमें बैठे हैं।...कुमार नित्यानन्द सिंह की यह जबर्दस्ती वे जीवन-भर नहीं भुला पाएँगे।...
मन्मथ बाबू ने एक उचटती-सी दृष्टि उन पर डाली और अनमने-से बैठ गए। उन्हें टालने का एक ही मार्ग था कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। वे समझ रहे थे कि आगंतुकों के प्रति उनका व्यवहार बहुत शिष्ट नहीं था; किंतु वे क्या करते ? जो लोग उन्हें प्रिय नहीं लगते ? उनसे बात, करने के लिए उनके मन में कोई भाव ही नहीं उगता। और ये लोग तो बलात् उनके घर में घुस आए थे और अब उनके सामने आ बैठे थे।.... इतने ही साधु हैं तो जाएँ और अपने कमरे में ध्यान करें।...
मन्मथ बाबू ने पास रखी एक पुस्तक उठा ली...वे पढ़ते रहेंगे तो ये लोग अपनी उपेक्षा मानकर स्वयं ही उठ जाएँगे। रूठकर उनके घर से ही चले जाएँ तो और भी अच्छा है।...
‘‘आप यह कौन-सी पुस्तक पढ़ रहे हैं ?’’ सहसा पहले साधु ने सीधे मन्मथ बाबू से ही पूछ लिया। मन्मथ बाबू के मन में एक मिश्रित-सी प्रतिक्रया हुई....किंतु यही अवसर था कि वे उसे उसका स्थान दिखा सकते थे...
‘‘बौद्ध धर्म पर लिखी गई एक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद है।’’ मन्मथ बाबू के स्वर में स्पष्ट व्यंग्य था, ‘‘कुछ पढ़े-लिखे भी हैं ? अंग्रेजी आती है ?’’
‘‘थोड़ी-थोड़ी।’’ साधु मुस्कराकर बाँग्ला में ही बोला, ‘‘अंग्रेजी जानने से ही कोई पढ़ा लिखा हो जाता है ?’’
‘‘क्यों ? पढ़-लिखकर ही तो अंग्रेजी आती है।’’ मन्मथ बाबू ने कुछ आवेश में कहा ।
‘‘नहीं ऐसे बहुत सारे अंग्रेज और अमेरिकी है जो तनिक भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, किंतु उनको अंग्रेजी आती है।’’ साधु ने कहा।
मन्मथ बाबू ने ध्यान से साधु की ओर देखाः वह वैसा मूर्ख भिखारी नहीं था, जैसा मन्मथ बाबू समझे बैठे थे। फिर भी उनके पढ़े-लिखे होने की संभावना से मन्मथ बाबू को किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हुई। उलटे उनकी खीज की आग को हवा दे गई।...यह कैसे संभव है ?...संन्यासी होकर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ता; और अंग्रेजी पढ़कर कोई संन्यासी नहीं होता।...
‘‘ठीक है, पर भारत में ऐसा नहीं होता।’’ मन्मथ बाबू ने स्वयं को सँभाला, ‘‘मैं मान लेता हूँ कि आप पढ़े-लिखे हैं।...तो महात्मा बुद्ध के विषय में भी कुछ जानते होंगे ? नाम तो सुना ही होगा ?’’ उन्होंने प्रश्न अंग्रेजी में ही किया था। अभी इस पाखंडी की पोल खुल जाती है।
‘‘कौन हिंदू उनके विषय में नहीं जानता।’’ साधु ने अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की।
‘‘आपका उनके विषय में क्या विचार है ?’’ मन्मथ बाबू साधु को घेर लेना चाहते थे।
‘‘सर्वभूतों के प्रति और विशेष कर अज्ञानी और दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति में ही तथागत का महान् गौरव सन्निहित होता है।’’ संन्यासी ने परिष्कृत अंग्रेजी में कहा, ‘‘बुद्ध के धर्मोंपदेश के समय संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गई थी। वह उस समय केवल पंडितों के ग्रंथों की ही भाषा थी। बुद्धदेव के कुछ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत में करना चाहा था, पर बुद्धदेव उनसे सदा यही कहते, ‘‘मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ, अतः मुझे जनभाषा में ही बोलने दो।’ और उसी कारण से उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन भाषा में ही पाए जाते हैं।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book